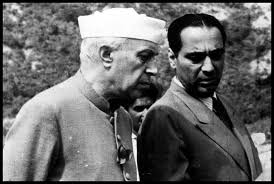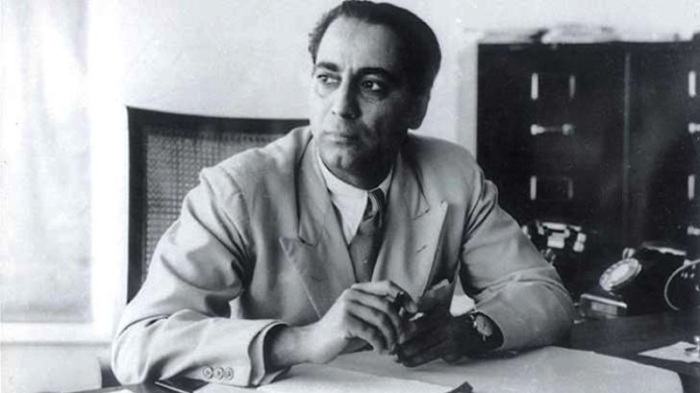![चंद्रयात्री बज आल्ड्रीन तथा नील आर्मस्ट्रांग नासा के प्रशिक्षण केंद्र मे चंद्रमा और लैंडर माड्युल के माडेल के साथ]()
चंद्रयात्री बज आल्ड्रीन तथा नील आर्मस्ट्रांग नासा के प्रशिक्षण केंद्र में लूनर लैंडर माड्युल के मॉडल के साथ[
वर्तमान मे कांसपिरेसी थ्योरियाँ एक बहुत बड़ा बाजार है और इस बाजार में कई तरह की कांसपिरेसी थ्योरी प्रचलित है जिनमे से एक है अपोलो चंद्रयात्रा षडयंत्र (कांसपिरेसी थ्योरी)। इस थ्योरी में ऐसे बहुत से लोग है जो यह मानते हैं कि मानव कभी चंद्रमा पर गया ही नहीं था।
अपोलो चंद्रयात्रा षडयंत्र (Moon Landing Conspiracy Theories) के अनुसार अपोलो अभियान का कुछ भाग या संपूर्ण अभियान ही झूठा था, इसे नासा ने कुछ अन्य संस्थाओ की सहायता से किसी फ़िल्म स्टूडियो में फ़िल्माया था। सबसे महत्वपूर्ण दावा यह है कि 1969 से 1972 के मध्य में सम्पन्न हुए छह चंद्रयानो के द्वारा 12 चंद्रयात्री चंद्रमा पर कभी गये ही नही थे। बहुत से समूह और व्यक्ति इस तरह के दावे 1970 के दशक के मध्य से कर रहे है कि नासा और अन्य संस्थाये आम जनता को गुमराह कर रहे है तथा वे गलत सबूतो को जनता के सामने दे रहे है। वे यह भी कहते है कि नासा फोटोग्राफ़िक प्रमाणो, टेलीमेट्री टेप्स, रेडीयो तथा टीवी प्रसारण रिकार्डींग, चंद्रमा की चट्टानो के नमूनो को नष्ट कर रहा है, तथा मुख्य गवाहों की हत्या कर रहा है, जिससे नासा का कथित झूठ पकड़ा ना जा सके।
चंद्रमा पर मानव के अवतरण के कई तृतीय पक्ष के प्रमाण भी उपलब्ध है, जिनका नासा से कोई संबंध नही है। इन कांसपिरेसी थ्योरी के दावो का कई बार , बहुत से समूहो/व्यक्तियों द्वारा विस्तृत रूप से खंडन किया जा चुका है। 2000 के बाद से नासा के अतिरिक्त कई अन्य अंतरिक्ष संस्थानो द्वारा चंद्रमा के उस क्षेत्र के जहां इन अभियानों के रॉकेट उतरे वहाँ के अत्याधिक उच्च गुणवत्ता(High Definition) वाले चित्र लिये जा चुके है जो आम जनता के लिये उपलब्ध है। इनमे अपोलो 11 के अतिरिक्त सभी चंद्र अभियानो द्वारा गाड़े गये अमरीकी झंडे अभी भी वहाँ मौजूद है, अपोलो 11 वाला अमरीकी ध्वज , चंद्रयात्रा से वापसी के समय वाले राकेट प्रज्वलन से उखड़ गया था।
![कांसपिरेसी थ्योरी एक बड़ा व्यवसाय बन चुका है, इन थ्योरी पर आधारित पुस्तके लिखी जाती है, उनकी बिक्री होती है। टीवी पर डाक्युमेंट्री दिखाई जाती है और उसके विज्ञापनो से कमाई होती है। इंटरनेट के जमाने मे ऐसी कांसपिरेसी थ्योरी की बदौलत वेबसाईट चलती है, विज्ञापन से आय होती है। युट्युब जैसे विडियो चैनल पर अधिक लोगो को आकर्षित करने मे इस तरह की कांसपिरेसी थ्योरी बड़ा आकर्षण होती है।]()
कांसपिरेसी थ्योरी एक बड़ा व्यवसाय बन चुका है, इन थ्योरी पर आधारित पुस्तकें लिखी जाती है, उनकी बिक्री होती है। टीवी पर डाक्युमेंट्री दिखाई जाती है और उसके विज्ञापनो से कमाई होती है। इंटरनेट के जमाने मे ऐसी कांसपिरेसी थ्योरी की बदौलत वेबसाईट चलती है, विज्ञापन से आय होती है। युट्युब जैसे विडियो चैनल पर अधिक लोगो को आकर्षित करने मे इस तरह की थ्योरियों का बड़ा हाथ होता है
कांसपिरेसी थ्योरी वाले व्यक्तियों/समूहो के अपने पूर्वनिर्धारित लक्ष्य होते है जिनमे पुस्तको/विडियो/डाकुमेंट्री की बिक्री, युट्युब/इंटरनेट/टीवी पर विज्ञापनो से होने वाली आय प्रमुख है, स्पष्ट और तृतिय पक्ष वाले प्रमाणो के होने के बावजूद ये लोग इस मुद्दे को 40 वर्षो से अधिक जीवित रखे हुये है। इनमे कुछ लोकप्रिय टीवी चैनल भी है जिसमे फ़ाक्स टीवी(Fox TV) प्रमुख है और उसने 2001 मे एक बहुप्रसिद्ध वृत्तचित्र (Conspiracy Theory: Did We Land on the Moon?) प्रसारित किया था , जिसमे यह दावा किया गया था कि नासा ने रूस से अंतरिक्ष दौड जीतने के लिये 1969 मे अपोलो 11 अभियान का नाटक किया था।
कांसपिरेसी थ्योरी की शुरुवात
1976 मे अमरीकी नौसेना के अफ़सर बिल कायसींग(Bill Kaysing) ने अपने प्र्काशन से एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसका नाम था “Never Went to the Moon: America’s Thirty Billion Dollar Swindle“। बिल कायसींग अंग्रेजी विषय से कला क्षेत्र (Bachelor of Arts in English) से स्नातक थे जिन्हें राकेट की कार्यप्रणाली के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसके बावजूद 1956 मे सैटर्न V राकेट मे प्रयुक्त होने वाले F-1 इंजन बनाने वाली कंपनी राकेटडाईन(Rocketdyne) ने उन्हें तकनीकी लेखक(Technical Writer) की नौकरी दी थी। इस नौकरी मे उन्हे इंजीनियरो की सहायता से भिन्न प्रयोग, उपकरण की कार्य विधि का तकनीकी लेखन करना होता था। उन्होने 1963 तक इस कंपनी के तकनीकी प्रकाशन विभाग का नेतृत्व किया। उन्होने अपनी इस पुस्तक मे नासा पर कई आरोप लगाये और उन्होने दावा किया कि अपोलो अभियान ने चंद्रमा पर अवतरण किया ही नही। उनके अनुसार चंद्रमा पर सफ़ल मानव अभियान की संभावना केवल 0.0017% ही थी। उनके अनुसार सोवियत संघ (USSR) की कड़ी निगरानी के बावजूद नासा के चंद्रमा पर जाने की बजाय उसका नाटक करना अधिक आसान था।
1980 मे धरती को चपटी मानने वालो का समूह फ़्लैट अर्थ सोसायटी(Flat Earth Society) ने नासा पर चंद्रमा पर मानव अवतरण की अफ़वाह फ़ैलाने का आरोप लगाया। उन्होने कहा कि यह सारा अभियान वाल्ट डिजनी के फ़िल्म स्टूडीयो मे फ़िल्माया गया था, जिसकी सारी स्क्रिप्ट विज्ञान फ़तांशी लेखक आर्थर सी क्लार्के(Aurther C Clarke) ने लिखी थी और निर्देशन स्टेनली कुब्रिक (Stanley Kubrick) ने किया था। एक अन्य कांस्पिरेसी लेखिका लिंडा देघ ने कहा कि नासा का अपोलो अभियान लेखक निर्देशक पीटर ह्यम्स(Peter Hyams) की फ़िल्म कैप्रीकोर्न वन(Capricorn One) से मिलता है,जिसमे अंतरिक्ष यान से मंगल की यात्रा दिखाई गई है जोकि अपोलो यान से मिलता जुलता है।
इसके बाद ऐसे दर्जनो कांसपिरेसी थ्योरी लेखक सामने आये और ढेर सारी किताबे लिखी गई, कुछ वृत्तचित्र(Documentary) भी बने।
षडयंत्र थ्योरी के अनुसार नासा तथा अमरीका का उद्देश्य
इस कांसपिरेसी थ्योरी को मानने वालो के अनुसार नासा और अमरीका के पास इस ड्रामा को करने के लिये कई उद्देश्य थे। इनमे ये तीन उद्देश्य प्रमुख है।
अंतरिक्ष दौड़
सं रा अमरीका के लिये सबसे बड़ी चुनौती सोवियत संघ और उसके साथ चल रहा शीत युद्ध था। चंद्रमा पर मानव अवतरण अमरीका को विश्व व्यापक राष्ट्रीय तथा तकनीकी सफ़लता दिलाता और उन्हे सबसे आगे दिखाता। लेकिन चंद्रमा पर जाना खतरनाक और महंगा अभियान था, जैसा जान एफ़ केनेडी द्वारा 1962 मे दिये गये भाषण मे भी कहा गया था कि हमने चंद्रमा पर जाना चुना क्योंकि यह कठिन था।
इस कांसपिरेसी थ्योरी के विरोधी फ़िल प्लेट अपनी पुस्तक बैड आस्ट्रोनामी मे लिखते है कि सोवियत संघ के पास अपना प्रतिस्पर्धी चंद्र अभियान था, उनके पास एक बहुत बड़ा इंटेलीजेंस नेटवर्क था, तथा उनके पास नासा के आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिये सक्षम वैज्ञानिको की फ़ौज थी। यदि नासा ने इस चंद्रमा पर मानव अभियान का ड्रामा रचा होता तो सोवियत संघ उसे झूठा प्रमाणित करने मे सक्षम था और उसने भंडाफ़ोड़ करने मे देर नही लगाई होती। वह भी उस स्थिति मे जब सोवियत संघ का अपना अभियान असफ़ल रहा था।
![बार्ट सिबरेल(Bart Sibrel) जब बज आल्ड्रीन को परेशान कर बाइबल पर हाथ रख कर कसम खाने कह रहे थे, तब आल्ड्रीन ने उन्हे एक घूंसा मारा था। इस मामले मे अदालत ने माना था कि गलती बार्ट सीब्रेल की थी और वे आल्ड्रीन को नाहक परेशान कर रहे थे।]()
बार्ट सिबरेल(Bart Sibrel) जब बज आल्ड्रीन को परेशान कर बाइबल पर हाथ रख कर कसम खाने कह रहे थे, तब आल्ड्रीन ने उन्हे एक घूंसा मारा था। इस मामले मे अदालत ने माना था कि गलती बार्ट सीब्रेल की थी और वे आल्ड्रीन को नाहक ही परेशान कर रहे थे।
कांसपिरेसी थ्योरिस्ट बार्ट सिबरेल(Bart Sibrel) ने जवाब दिया कि सोवियत संघ के पास 1972 तक गहन अंतरिक्ष मे अंतरिक्षयान को ट्रेक करने की क्षमता नही थी। जैसे ही उनके पास यह क्षमता आई बचे तीन अपोलो अभियान रद्द कर दिये गये। बार्ट सिबरेल का यह जवाब एक सफ़ेद झूठ था। सोवियत संघ चंद्रमा तक मानवरहित अभियान 1959 से भेज रहा था तथा गहन अंतरिक्ष मे अंतरिक्षयानो को ट्रेक करने की क्षमता उनके पास 1962 से IP-15 तथा IP-16 के रूप मे क्रमश उस्सुर्जिस्क(Ussurjisk) तथा आईपटोर्जा(Eypatorja) उपग्रहो मे थी। सोवियत संघ ने अपोलो अभियान के यानो को स्पेस ट्रांसमिशन कार्प्स से ट्रेक किया था जोकि इस तरह के अभियानो पर नजर रखने के लिये पूरी तरह से उपकरणो और तकनीक से पूरी तरह लैस था। वैसीली मिशिन(Vasily Mishin) ने यह संपूर्ण विवरण एक लेख “The Moon Programme That Faltered” मे दिया है, यह लेख बताता है कि नासा द्वारा चंद्रमा पर सफ़ल मानव अवतरण के बाद सोवियत संघ का चंद्रमा अभियान कैसे बिखर गया।
अपोलो अभियान के अंतिम तीन अभियानों के रद्द होने की घोषणा दो वर्ष पहले 1970 मे ही खर्च पर कटौती के मद्देनजर कर दी गई थी।
नासा बजट और प्रतिष्ठा
कांसपिरेसी थ्योरी समर्थको के अनुसार नासा ने चंद्रमा पर मानव भेजने का ड्रामा अपनी बेइज्जती से बचने और बजट की आपूर्ति जारी रखने के लिये किया था। नासा को चंद्रमा अभियान के लिये 30 अरब डालर मिले थे, बिल कायसिंग ने अपनी पुस्तक मे लिखा था कि इन पैसो का प्रयोग बहुत से लोगो के मुंह बंद रखने के लिये किया गया था। अधिकतर कांसपिरेसी थ्योरी समर्थक मानते है कि उस समय की तकनीक से चंद्रयात्रा असंभव थी और जान एफ़ केनेडी द्वारा 1961 मे दशक के अंत तक चंद्रमा से मानव के सकुशल लौट कर आने के लक्ष्य को पूरा करने के लिये इस ड्रामा को पूरा करना आवश्यक था। तथ्य यह है कि 1973 मे नासा द्वारा अमरीकी कांग्रेस मे दिये गये खातो के अनुसार इस अभियान मे कुल 25.4 अरब डालर खर्च हुये थे।
मेरी बेन्नेट(Maru Bennet) तथा डेवीड पर्सी(David Percy) ने अपनी किताब “डार्क मून: अपोलो एन्ड द व्हिशल ब्लोवर्स(Dark Moon: Apollo and the Whistle-Blowers)” मे लिखा है कि सभी ज्ञात और अज्ञात खतरो को जानते हुये नासा अंतरिक्ष यात्रीयों के टीवी पर सीधे प्रसारण पर बीमार होने या मृत्यु होते दिखाने का खतरा कभी नही उठाती। लेकिन इसके विरोध मे यह भी एक तथ्य है कि नासा को इससे बड़ी शर्मिंदगी उस समय उठानी पड़ी थी जब उसके तीन अंतरिक्ष यात्री ज़मीन पर ही अपोलो 1 की जांच के दौरान जलकर मर गये थे। इस दुर्घटना के बाद नासा के सभी वरिष्ठ अधिकारीयों को सिनेट तथा संसद की कमेटी के समक्ष पेश होना पड़ा था। साथ ही तकनीकी सीमाओं के कारण उस समय यानो की उड़ान और अवतरण के दौरान सीधे प्रसारण की सुविधा उपलब्ध नही थी।
वियतनाम युद्ध
2009 मे अमेरीकन पैट्रिआट फ़्रेंड्स नेटवर्क ने दावा किया था कि चंद्र अभियानों ने जनता का ध्यान अलोकप्रिय वियतनाम युद्ध से हटाने मे मदद की और वियतनाम युद्ध की समाप्ति के साथ ही भविष्य के चंद्र अभियानों को रद्द कर दिया गया। जबकि यह सच नही है, अभियानों को समाप्त करने की योजना दो वर्ष पहले ही बन गई थी। अमेरिकी युद्ध बजट नासा के बजट का प्रतिस्पर्धी था। नासा को सबसे अधिक बजट 1966 मे आवंटित हुआ था जबकि 1972 मे वह 42.3% कम हो गया था। यह एक कारण था कि ना केवल अपोलो 18,19 तथा 20 के अभियान रद्द हुये थे बल्कि स्थाई अंतरिक्ष स्टेशन(permanent space station) की योजना, मानव मंगल अभियान भी रद्द हो गये थे।
चंद्र अभियान षडयंत्र के समर्थन के (कु) तर्क और उनका खंडन
![कुछ वैज्ञानिक जैसे आर्गोने राष्ट्रीय प्रयोगशाला(Argonne National Laboratory ) के विंस काल्डर(Vince Calder) तथा एंड्र्यु जानसन ने इन कांसपिरेसी थ्योरी के समर्थको के कुतर्को का उत्तर दिया है। इसके अनुसार नासा द्वारा इस अभियान की जानकारी पूर्णत सत्य है और इस कांसपिरेसी थ्योरी के समर्थको द्वारा उठाये गये मुद्दे विज्ञान की मूलभूत समझ ना होने से उपजी गलतफ़हमीयाँ है।]()
कुछ वैज्ञानिक जैसे आर्गोने राष्ट्रीय प्रयोगशाला(Argonne National Laboratory ) के विंस काल्डर(Vince Calder) तथा एंड्र्यु जानसन ने इन कांसपिरेसी थ्योरी के समर्थको के कुतर्को का उत्तर दिया है। इसके अनुसार नासा द्वारा इस अभियान की जानकारी पूर्णत सत्य है और इस कांसपिरेसी थ्योरी के समर्थको द्वारा उठाये गये मुद्दे विज्ञान की मूलभूत समझ ना होने से उपजी गलतफ़हमीयाँ है।
चंद्र अभियान को नाटक दिखाने वाली कई कांसपिरेसी थ्योरी बनाई गई है जिसके अनुसार या तो चंद्रमा पर अवतरण नही हुआ और नासा ने झूठ बोला या चंद्रमा पर लैंडीग हुई लेकिन उस तरह से नही जिस तरह से बताया गया है। ये लोग इन अभियानों के तथ्यो के मध्य सुराख खोजने का प्रयास करते है। इसमे सबसे लोकप्रिय आईडीया इस अभियान के आरंभ से अंत तक का झूठा होना है। इनमे से कुछ दावो के अनुसार उस समय की तकनीक मानव को चंद्रमा तक भेजने मे अक्षम थी और पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य की वान एलन बेल्ट विकिरण पट्टी(Van Allen radiation belts), सौर ज्वाला(solar flares), सौर वायु(solar wind), कोरोनल मास इजेक्शन(coronal mass ejections) और ब्रह्मांडीय विकिरण(cosmic rays) इस तरह की यात्राओ को असंभव बनाती है।
कुछ वैज्ञानिक जैसे आर्गोने राष्ट्रीय प्रयोगशाला(Argonne National Laboratory ) के विंस काल्डर(Vince Calder) तथा एंड्र्यु जानसन ने इन कांसपिरेसी थ्योरी के समर्थको के कुतर्को का उत्तर दिया है। इसके अनुसार नासा द्वारा इस अभियान की जानकारी पूर्णत सत्य है और इस कांसपिरेसी थ्योरी के समर्थको द्वारा उठाये गये मुद्दे विज्ञान की मूलभूत समझ ना होने से उपजी गलतफ़हमीयाँ है।
अब हम चर्चा करते है कांसपिरेसी थ्योरी के समर्थको द्वारा उठाये गये मुद्दो की और उनका एक के बाद एक विश्लेषण करते है।
षडयंत्रकारीयों की संख्या
परड्यु विश्वविद्यालय(Purdue Universi ty) के वैमानिकी अभियांत्रीकी प्रोफ़ेसर जेम्स लांगस्की(James Longuski)के अनुसार इस पैमाने पर कोई भी षडयंत्र अपने आकार और जटिलताओं के कारण सफ़ल नही हो सकता है।
![एक छोटे षडयंत्र वाटरगेट स्कैंडल को गुप्त नही रखा जा सका था जिसमे गिनती के लोगो का समावेश था जबकि इसमे तो इतने अधिक लोग जुड़े हुये है कि कोई ना कोई बाहर निकल कर अब तक पूरा भंडाफ़ोड़ कर देता।]()
एक छोटे षडयंत्र वाटरगेट स्कैंडल को गुप्त नही रखा जा सका था जिसमे गिनती के लोगो का समावेश था जबकि इसमे तो इतने अधिक लोग जुड़े हुये है कि कोई ना कोई बाहर निकल कर अब तक पूरा भंडाफ़ोड़ कर देता।
अपोलो अभियान मे दस वर्ष के दौरान 400,000 से अधिक व्यक्तियों ने कार्य किया था। इस अभियान मे अपोलो 11,12,14,15,16 तथा 17 द्वारा हुई उड़ानों में कुल 18 व्यक्ति धरती से चाँद की ओर गए, इनमें से 12 व्यक्तियों ने चंद्रमा पर कदम रखे, 6 व्यक्ति उन के साथ चंद्रमा की कक्षा मे कमांड माड्युल के पायलट के रूप मे गये थे, कमांड मॉड्यूल के ये छह यात्री चंद्रमा की परिक्रमा कर वापस आये थे। अपोलो १३ के यात्री यान में आई तकनीकी खराबी के कारण चंद्रमा पर अवतरण नही कर पाये और चंद्रमा की परिक्रमा कर वापस आ गये। लाखो लोगो द्वारा जिसमे अंतरिक्ष यात्री, वैज्ञानिक, इंजीनियर, तकनीकीशियन और कुशल श्रमजीवी द्वारा इस अभियान को गुप्त रखना होगा। इस तरह के विशाल षडयंत्र को गुप्त रखने की बजाय चंद्रमा पर यान भेजकर उन्हे सकुशल वापस लाना अधिक आसान है। आज तक अमरीकी सरकार या नासा मे से एक व्यक्ति ने भी इस अभियान को षडयंत्र नही कहा है।
2005 मे प्रसिद्ध टीवी कार्यक्रम पेन एन्ड टेलर: बुलशीट!(Penn & Teller: Bullshit) के एक एपिसोड मे पेन जिलेट ने कहा था कि एक छोटे षडयंत्र वाटरगेट स्कैंडल को गुप्त नही रखा जा सका था जिसमे गिनती के लोगो का समावेश था जबकि इसमे तो इतने अधिक लोग जुड़े हुये है कि कोई ना कोई बाहर निकल कर अब तक पूरा भंडाफ़ोड़ कर देता।
इस अभियान के फोटोग्राफ़ो का विश्लेषण
कांसपिरेसी थ्योरीस्ट नासा के द्वारा प्रकाशित चित्रो के पीछे लगे रहते है और चंद्रमा पर लिये गये फोटो मे विसंगतियाँ खोजते रहते है। फ़ोटोग्राफ़ी विशेषज्ञ जिनमे नासा से असंबधित विशेषज्ञ भी शामिल है इन विसंगतियों के बारे मे कहते है कि यह वह विसंगतियाँ है जो वास्तविक चंद्र अभियान मे ही पाई जा सकती है, इस तरह की विसंगतियाँ किसी स्टुडियो मे ली गई फोटो मे नही आ सकती। कांसपिरेसी थ्योरीस्ट के उठाये गये मुख्य मुद्दे और उनका निराकरण नीचे है
1. क्रासहेयर कुछ चित्रो मे क्रासहेयर वस्तुओं के पिछे दिखाई दे रहा है। इस अभियान के कैमरो के लेंस के सामने एक कांच लगा था जिसपर क्रास हेयर बना हुआ होता है। इस तरह के कैमरो से लिये चित्रो मे क्रासहेयर वस्तुओं के सामने दिखना चाहीये। यह दर्शाता है कि ये वस्तुये उन चित्रो मे उपर से चिपकाई गई है।
निराकरण : यह विसंगति केवल पुन:मुद्रित तथा स्कैन के चित्रो मे ही है, वास्तविक चित्रो मे नही है। यह विसंगति ओवरएक्सपोजर से आती है जिसमे चमकीला सफ़ेद हिस्सा पतले काले क्रासहेयर को दबा देता है जोकि 0.1 मीमी चौड़े ही होते है। इसके अतिरिक्त बहुत से चित्र ऐसे है जिनमे क्रासहेयर का मध्य वाला हिस्सा ही धुल गया है जबकि बाकी हिस्सा ज्यों का त्यों है। कुछ चित्रो मे यह क्रासहेयर अमरीकी ध्वज के लाल रंग वाले हिस्से मे दिख रहा है जबकि सफ़ेद रंग वाले हिस्से मे दब गया है। अब केवल सफ़ेद पट्टियों वाले हिस्से को चिपकाने का तो कोई तुक नही बनता है।
चित्र 5-2004 के अधिक गुणवत्ता वाले चित्र का स्कैन जिसमे क्रासहेयर तथा लाल पट्टी स्पष्ट है।
![1998 के कम गुणवत्ता वाले चित्र का स्कैन जिसमे क्रासहेयर तथा लाल पट्टी दब गई है।]()
1998 के कम गुणवत्ता वाले चित्र का स्कैन जिसमे क्रासहेयर तथा लाल पट्टी दब गई है।
![2004 के अधिक गुणवत्ता वाले चित्र का स्कैन जिसमे क्रासहेयर तथा लाल पट्टी स्पष्ट है।]()
2004 के अधिक गुणवत्ता वाले चित्र का स्कैन जिसमे क्रासहेयर तथा लाल पट्टी स्पष्ट है।
![अपोलो 15 के चंद्रयात्री डेवीड स्काट अमरीकी ध्वज को सैल्युट करते हुये। इस चित्र मे क्रासहेयर ध्वज की सफ़ेद पट्टी पर स्पष्ट नही है।]()
अपोलो 15 के चंद्रयात्री डेवीड स्काट अमरीकी ध्वज को सैल्युट करते हुये। इस चित्र मे क्रासहेयर ध्वज की सफ़ेद पट्टी पर स्पष्ट नही है।
![ध्वज का आवर्धित चित्र जिसमे सफ़ेद भाग पर क्रास हेयर दब गया है।]()
ध्वज का आवर्धित चित्र जिसमे सफ़ेद भाग पर क्रास हेयर दब गया है।
2. घुमे हुये क्रास हेयर कुछ चित्रो मे क्रासहेयर घुमे हुये है या गलत जगह पर है।
निराकरण : यह कुछ लोकप्रिय चित्रो को काटने(crop) तथा सुंदरता के लिये घूमा कर प्रस्तुत करने की वजह से है।
3.चित्रो की गुणवत्ता उम्मीद से अधिक अच्छी है।
निराकरण : अपोलो अभियान के बहुत सी खराब गुणवत्ता वाले चित्र भी है। लेकिन नासा द्वारा सर्वोत्तम चित्रो को ही प्रकाशित किया है और यह स्वाभाविक भी है कि आप अपने बेहतरीन चित्रो को ही प्रकाशित करेंगे। साथ मे अपोलो अभियान मे अंतरिक्षयात्रीयों ने अधिक रिजाल्युशन वाले हैसलब्लेड 500 EL कैमरो का प्रयोग किया था जिसमे सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले कार्ल जियस ओप्टिक्स तथा 70 मीमी की फ़िल्म का प्र्योग किया था।
4: चित्रो मे तारे : अभियान के चित्रो मे तारे नही दिखाई दे रहे है। अपोलो 11 के यात्रीयों ने संवाददाता सम्मेलन मे तारो के दिखाई देने की बात याद ना होने का कहा था।
निराकरण :
![फ़रवरी 2008 मे अंतरिक्ष स्पेस शटल द्वारा अंतराष्टीय अंतरिक्ष केंद्र का चित्र जिसमे तारे दिखाई नही दे रहे है।]()
फ़रवरी 2008 मे अंतरिक्ष स्पेस शटल द्वारा अंतराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र का चित्र जिसमे तारे दिखाई नही दे रहे है।
![जुन 1995 पृथ्वी और मीर, तारे दिखाई नही दे रहे है।]()
जुन 1995 पृथ्वी और मीर का चित्र जिसमे तारे दिखाई नही दे रहे है।
![अपोलो 16 अभियान मे एक विशेष पराबैंगनी किरणो(far ultraviolet camera) से लिया चित्र जिसमे पृथ्वी और तारे दिखाई दे रहे है।]()
अपोलो 16 अभियान मे एक विशेष पराबैंगनी किरणो(far ultraviolet camera) से लिया चित्र जिसमे पृथ्वी और तारे दिखाई दे रहे है।
![स्पेस शटल अटलांटिस द्वारा लिया लंबे एक्सपोजर वाला चित्र(1.6 seconds at f/2.8, ISO 10000)]()
स्पेस शटल अटलांटिस द्वारा लिया लंबे एक्सपोजर वाला चित्र(1.6 seconds at f/2.8, ISO 10000)
5. छायाओं का कोण और रंग : चंद्रमा पर की चित्रो मे छायाओं का कोण और रंग सही नही है। इससे यह लगता है कि इन चित्रो को किसी स्टुडियो मे लिया गया है जिसमे एक से अधिक प्रकाश स्रोतो क प्रयोग किया गया है।
निराकरण : चंद्रमा की सतह पृथ्वी के जैसे नही है। चंद्रमा की सतह चमकीली है और इस उबड़खाबड़ सतह पर छाया और प्रकाश के परावर्तन से छायाओं के शेड्स एक जैसे नही बनतेहै। छायाओं के रंग पर सतह द्वारा परावर्तित प्रकाश, चौडे कोण वाले कैमरा लेंस(Wide angle lens) द्वारा उत्पन्न विकृति तथा चंद्रमा की धूल का भी प्रभाव पड़ता है। जब ये चित्र लिये गये उस समय एक से अधिक प्रकाश स्रोत भी थे जिसमे सूर्य, पृथ्वी द्वारा परावर्तित सूर्य प्रकाश, चंद्रमा की सतह, अंतरिक्ष यात्रीयों के सूट तथा लुनर माड्युल द्वारा द्वारा परावर्तित प्रकाश का समावेश है। इन सभी स्रोतो द्वारा परावर्तित प्रकाश छाया वाले भागो मे पड़ने से उनके भिन्न भिन्न शेड्स दिखाई देंगे।
छायाओं के कोण और लंबाई मे विसंगतियाँ : चंद्रमा के क्रेटरों तथा पहाड़ीयों पर पड़ने वाली छाया लंबी, छोटी या विकृत प्रतित हो सकती है।
इस कुतर्क का खंडन लोकप्रिय टीवी धारावाहिक MythBusters के एपिसोड “NASA Moon Landing” मे किया गया है।
![कांसपिरेसी थ्योरीस्ट कहते है कि अपोलो अभियान के चित्रो मे छाया समांतर नही है।]()
कांसपिरेसी थ्योरीस्ट कहते है कि अपोलो अभियान के चित्रो मे छाया समांतर क्यों नही है।
नीचे दिया गया चित्र पृथ्वी पर है, इसमे आप देख सकते है कि एक ही प्रकाश स्रोत सूर्य के होने के बावजूद छाया समांतर ना होकर अलग कोण बना रही है। इस तरह का प्रभाव सतह के समतल ना होने से उत्पन्न होता है जिससे टीले, गड्डो के कारण छाया संमातर ना होकर कोण बनाते है।
![नीचे दिया गया चित्र पृथ्वी पर है, इसमे आप देख सकते है कि एक ही प्रकाश स्रोत सूर्य के होने के बावजूद छाया समांतर ना होकर अलग कोण बना रही है। इस तरह का प्रभाव सतह के समतल ना होने से उत्पन्न होता है जिससे टीले, गड्डो के कारण छाया संमातर ना होकर कोण बनाते है।]()
यह चित्र पृथ्वी पर है, इसमे आप देख सकते है कि एक ही प्रकाश स्रोत सूर्य के होने के बावजूद छाया समांतर ना होकर अलग कोण बना रही है। इस तरह का प्रभाव सतह के समतल ना होने से उत्पन्न होता है जिससे टीले, गड्डो के कारण छाया संमातर ना होकर कोण बनाते है।
![यह गया चित्र पृथ्वी पर है, इसमे आप देख सकते है कि एक ही प्रकाश स्रोत सूर्य के होने के बावजूद छाया समांतर ना होकर अलग कोण बना रही है। इस तरह का प्रभाव सतह के समतल ना होने से उत्पन्न होता है जिससे टीले, गड्डो के कारण छाया संमातर ना होकर कोण बनाते है।]()
यह चित्र भी पृथ्वी पर लिया है, इसमे आप देख सकते है कि एक ही प्रकाश स्रोत सूर्य के होने के बावजूद छाया समांतर ना होकर अलग कोण बना रही है। इस तरह का प्रभाव सतह के समतल ना होने से उत्पन्न होता है जिससे टीले, गड्डो के कारण छाया संमातर ना होकर अलग कोण बना रही है।
6. चित्रो की पृष्ठभूमी : बहुत से चित्रो मे एक जैसी ही पृष्ठभूमी है लेकिन चित्र विवरण के अनुसार वे कई मील के दूरी पर है। यह दर्शाता है कि इन चित्रो को किसी स्टूडियो मे किसी पेंट किये हुये पोस्टर के सामने लिया गया है।
निराकरण : इन चित्रो की पृष्ठभूमी एक जैसी नही है बल्कि एक जैसी दिखाई दे रही है। इसमे समीप की पहाड़ीयाँ दिखाई दे रही है वे वास्तविकता मे कई मील दूर पर स्थित पर्वत है। पृथ्वी पर दूर की वस्तुये धूंधली और अस्पष्ट दिखाई देती है लेकिन चंद्रमा पर वातावरण या कोहरा नही है जिससे वे दूरी पर भी उतनी ही साफ़ स्पष्ट दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त चंद्रमा पर दूरी के अनुमान की तुलना के लिये वस्तुये जैसे पेड़ नही है, जिससे चित्रो से यह पता नही चलता कि वे पास मे है या दूरी पर स्थित है।
7. चित्रो की अत्यधिक संख्या : लिये गये चित्रो की संख्या बहुत अधिक है। इतने अधिक चित्रो को लेने के लिये हर पचास सेकंड मे एक चित्र लिया जाना चाहिये।
निराकरण : चंद्रमा की सतह पर चित्र लेने के लिये कैमरे बहुत सरल थे और वे एक सेकंड मे दो चित्र ले सकते थे। हर पचास सेकंड मे एक चित्र लेने वाली गणना एक चंद्रयात्री को ध्यान मे रख कर की गई है लेकिन वास्तविकता मे दो चंद्रयात्री थे।
8. ’C’ मार्क की हुई चट्टान : एक मे एक चट्टान पर और उसके समीप के स्थल पर ’C’ लिखा हुआ है जो दर्शाता है कि किसी स्टूडियो मे यह सेट-अप किया गया था और वे लेबल ’C’ हटाना भूल गये।
निराकरण : “C” लेबल वाला चित्र मुद्रण की गलती है, यह वास्तविक फ़िल्म मे नही है। पूरी संभावना है कि चित्र मुद्रित होते समय मानव केश चित्र पर चिपक गया था।
![वास्तविक AS16-107-17445 चित्र]()
वास्तविक AS16-107-17445 चित्र
![वास्तविक AS16-107-17446 चित्र]()
वास्तविक AS16-107-17446 चित्र
![]()
AS16-107-17446 पुणमुद्रण वाला चित्र जिसमे मानव केश के कारण ’C’ दिख रहा है।
9. हाट स्पाटस(Hot spots)”: कुछ चित्रो मे स्टुडीयो के जैसे “हाट स्पाटस(Hot spots)” दिख रहे है जो दर्शाते है कि एक विशाल स्पाट्लाईट का प्रयोग किया गया होगा।
निराकरण : 1.चंद्रमा की सतह के गड्ढे किसी यातायात चिन्ह पर लगे कांच की गोलाकार सतह या ओस की बुंद या गीली घास के जैसे ही फ़ोकस बनाते है। इस प्रभाव से चित्र खींचने वाले की छाया के आसपास एक प्रभामंडल बनता है जो चित्र मे दिख रहा है।
2. यदि चंद्रयात्री सूर्यप्रकाश मे खड़ा होकर छायावाले हिस्से मे स्थित वस्तु का चित्र ले रहा हो तो चंद्रयात्री के सूट से परावर्तित प्रकाश स्पाटलाईट जैसे प्रभाव दिखायेगा।
3. अपोलो अभियान के कुछ प्रकाशित चित्र उच्च कांट्रास्ट(High Contrast) वाले मुद्रित चित्र है। वास्तविक चित्रो अधिक स्पष्ट है।
![अपोलो 11 अभियान मे बज आल्ड्रीन का वास्तविक चित्र]()
अपोलो 11 अभियान मे बज आल्ड्रीन का वास्तविक चित्र
![अपोलो 11 अभियान मे बज आल्ड्रीन का अधिक प्रचलित संपादित चित्र जिसमे स्पाटलाईट प्रभाव दिख रहा है।]()
अपोलो 11 अभियान मे बज आल्ड्रीन का अधिक प्रचलित संपादित चित्र जिसमे स्पाटलाईट प्रभाव दिख रहा है।
10.नील आर्मस्ट्रांग की चंद्रमा पर उतरते हुये चित्र :फोटो मे/विडियो मे नील आर्मस्ट्रांग की चंद्रमा पर उतरते हुये चित्र किसने लिया ?
निराकरण : यह चित्र लुनर माड्युल ने ही लिये। नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा की सतह पर उतरने से पहले ही लुनर माड्युल की एक बाजु से फोटो लेने वाले कैमरे तथा टीवी कैमरे वाले एक उपकरण को नीचे किया था। नील आर्मस्ट्रांग के चंद्रमा पर उतरने से पहले ही इस कैमरे ने चित्र लेना और पृथ्वी तक सीधे प्रसारण के लिये टीवी फ़ीड भेजना आरंभ कर दिया था।
वातावरण
1 . वान एलन विकिरण बेल्ट (Van Allen radiation belt) चंद्रयात्रीयों पृथ्वी से चंद्रमा और वापसी की यात्रा मे बचना संभव नही है क्योंकि मार्ग मे वान एलन विकिरण बेल्ट (Van Allen radiation belt) नामका घातक क्षेत्र है।
![वान एलेन बेल्ट]()
वान एलेन बेल्ट
निराकरण : दो मुख्य वान एलन विकिरण पट्टे है, आंतरिक पट्टा और बाह्य पट्टा और एक तीसरा संक्रमण पट्टा। इनमे से आंतरिक पट्टा अधिक घातक है जिसमे ऊर्जावान प्रोटान होते है, जबकि बाह्य पट्टे मे कम घातक इलेक्ट्रान है। अपोलो यान इस आंतरिक पट्टे को तेजी से कुछ ही मिनटों मे पार कर गये थे, जबकि उन्हे बाह्य पट्टे को पार करने मे आधा घंटा लगा था। अंतरिक्षयात्रीयों के इस घातक आयनाइजींग विकिरण(ionizing radiation) से बचाव के लिये यान के बाह्य भाग मे एल्युमिनियम की पत्री लगी थी। इसके साथ ही यान का पथ इस तरह से बनाया गया था कि यान पर इस विकिरण का न्यूनतम प्रभाव हो। इस पट्टे के शोधकर्ता जेम्स वान एलन ने ही इस यात्रा के अपोलो यान के लिये अत्यधिक घातक होने से इंकार किया था। खगोलशास्त्री फ़िल प्लेट के अनुसार इस यात्रा मे चंद्रयात्री पर पड़ने वाले विकिरण की मात्रा 1 rem (10msv) से कम थी जोकि समुद्री तट पर तीन वर्ष रहने पर पड़ने वाले विकिरण के तुल्य है। इस यात्रा मे चंद्रयात्रीयों द्वारा झेला गया कुल विकिरण किसी परमाणु संयंत्र मे एक वर्ष कार्य करने पर पड़ने वाले सुरक्षित विकिरण के तुल्य है और यह मात्रा किसी अंतरिक्ष शटल के यात्री पर पड़ने वाले विकिरण से ज्यादा अधिक नही है।
![अपोलो यात्रीयों पर विकिरण की मात्रा]()
अपोलो यात्रीयों पर विकिरण की मात्रा
2. इ्न विकिरण से सारी फ़ोटोग्राफ़िक फ़िल्मे एक्सपोज हो जानी चाहिये थी।
निराकरण : फ़िल्मो को इन विकिरण से एक्सपोज होने से बचाने के लिये धातुओं के डीब्बे मे रखा गया था। इसके अलावा रोबोटिक अभियान लुनर ओर्बिटर तथा लुना 3 मे फ़िल्मो को यान मे डेवलप किया जाता था इसलिये उनपर विकिरण से कोई प्रभाव नही पड़ा था।
3. कैमरा फ़िल्म चंद्रमा की सतह दिन के समय इतनी अधिक उष्ण हो जाती है कि कैमरा फ़िल्म पिघल जानी चाहिये।
निराकरण : चंद्रमा पर वातावरण नही है जिससे चंद्रमा की सतह की गर्मी उपकरणो तक संवहन द्वारा नही पहुंचती। चंद्रमा पर ऊष्मा के संचरण का इकलौता माध्यम विकिरण ही है। विकिरण से ऊर्जा के संवहन के भौतिकी को अच्छे से समझा जा चुका है और आप्टीकल कोटींग तथा उचित पेंट का प्रयोग इन कैमरा फ़िल्म को सही तापमान मे रखने और अत्याधिक उष्मा से बचाने के लिये पर्याप्त था। चंद्रयान का तापमान भी इसी तरह से नियंत्रण मे रखा गया था, उसे विकिरण उष्मा से बचाने के लिये सुनहरे रंग से पोता गया था।
इसके अतिरिक्त चंद्र अभियान सूर्योदय के समय पर ही रखे गये थे। ध्यान रहे कि चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के 29½ दिन के तुल्य होता है, जिसका अर्थ है कि चंद्रमा पर सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य लगभग पंद्रह दिन होते है। चंद्रमा पर लंबे अभियानों मे चंद्रयात्रियों ने उनके सूट की शीतलन प्रणाली पर अतिरिक्त दबाव महसूस किया था क्योंकि सूर्य और सतह का तापमान बड़ रहा था, लेकिन इस प्रभाव को वातावकूलन प्रणाली ने आसानी से नियंत्रण मे कर लिया था। जबकि कैमरा और उसकी फ़िल्मे सीधे सूर्य प्रकाश मे नही थी जिससे वह इतनी अधिक गर्म नही हुई कि उन्हे कोई नुकसान होता।
4.सौर ज्वाला :अपोलो 16 के यात्री अपने चंद्रमा की यात्रा के मार्ग एक विशाल सौर ज्वाला से बच नही सकते थे।
निराकरण : अपोलो 16 अभियान के दौरान कोई सौर ज्वाला उत्पन्न नही हुई थी। अगस्त 1972 मे एक विशाल सौर ज्वाला उत्पन्न हुई थी लेकिन अपोलो 16 पृथ्वी तक लौट चुका था और अपोलो 17 रवाना नही हुआ था।
5. ध्वज कैसे लहरा रहा है ? चंद्रमा पर वायु नही है लेकिन चंद्रमा पर गाड़ा गया अमरीकी ध्वज कैसे लहरा रहा था ? यह दर्शाता है कि इसे पृथ्वी पर फ़िल्माया गया है और हवा के झोंके से ध्वज लहरा रहा है।
निराकरण : ध्वज को एक सीधे डंडे मे नही एक Г- आकार के डंडे मे लगाया गया था, इसके कारण ध्वज नीचे नही हुआ था। ध्वज उसी समय लहराता दिख रहा है जब चंद्रयात्री उसे डंडे को घुमा घुमा कर चंद्रमा पर गाड़ रहे थे। ध्वज पर उसके भंडारण की वजह से सिलवटे थी। ये दोनो कारक स्थिर चित्र मे ध्वज लहराने का प्रभाव दिखा रहे है। यदि इस दौरान के वीडियो को देखे तो ध्वज के गाड़ देने के बाद सैल्युट करने दौरान वह स्थिर हो जाता है। इसे भी लोकप्रिय टीवी धारावाहिक मिथबस्टर(Mythbuster) के एपिसोड मे भी देखा जा सकता है।
![बज आल्ड्रीन का अमरीकी ध्वज को सैलयुट करते हुये चित्र]()
बज आल्ड्रीन का अमरीकी ध्वज को सैलयुट करते हुये चित्र
![कुछ सेकंड बाद बज आल्ड्रीन का अमरीकी ध्वज को सैलयुट करते हुये चित्र]()
कुछ सेकंड बाद बज आल्ड्रीन का अमरीकी ध्वज को सैलयुट करते हुये चित्र
![ध्यान दे: ध्वज मे कोई गतिविधि नही है! बज आल्ड्रीन का अमरीकी ध्वज को सैलयुट करते हुये चित्र का एनिमेशन]()
ध्यान दे: ध्वज मे कोई गतिविधि नही है! बज आल्ड्रीन का अमरीकी ध्वज को सैलयुट करते हुये चित्र का एनिमेशन
6. चंद्रयात्रीयों के पदचिह्न :चंद्रमा की धुल पर नमी नही है लेकिन चंद्रयात्रीयों के पदचिह्न बहुत अच्छे से छपे है।
निराकरण : चंद्रमा की धूल पर पृथ्वी के जैसे मौसम का प्रभाव नही है, वह रेत के जैसे खूरदूरी सतह, नुकीले कोणो वाले नही है। उसके धूलकण आपस मे आसानी से चिपककर एक आकार मे ढल जाते है। चंद्रयात्रीयों ने चंद्रमा की धुल को टैलकम पाउडर या गीली रेत सदृश कहा है।
इसे भी लोकप्रिय टीवी धारावाहिक मिथबस्टर के एपिसोड मे देखा जा सकता है।
![बज आल्ड्रीन द्वारा लिया चित्र]()
बज आल्ड्रीन द्वारा लिया चित्र
7. साउंड स्टेज/हार्नेस का प्रयोग: चंद्रमा पर अवतरण को किसी स्टेज पर या किसी दूरस्थ रेगिस्तान मे फ़िल्माया गया है जहाँ चंद्रयात्री या तो हार्नेस की सहायता से उछल उछल कर चले है या स्लो-मोशन फ़ोटोग्राफ़ी की सहायता से चंद्रमा पर होने का भ्रम उत्पन्न किया गया है।
निराकरण : 1. HBO के वृत्तचित्र “फ़्रोम द अर्थ टू द मून” तथा फ़िल्म अपोलो 13 मे स्टेज तथा हार्नेस का प्रयोग किया गया है। इन फ़िल्मो से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जब धूल उड़ती है तब वह जल्दी बैठती नही है, कुछ धूल एक बादल जैसा बनाती हौ। लेकिन अपोलो अभियान के विडियो फ़ुटेज मे चंद्रयात्रीयों के जूतो से तथा चंद्रबग्गी के पहियो से उड़ने वाली धूल चंद्रमा के कम गुरुत्व के कारण सतह से अधिक उंचाई तक उठती है तथा जल्दी ही एक पैराबिलिक पथ बनाते हुये सतह पर गिर जाती है क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल भी नही है। यदि इसका फ़िल्मांकन पृथ्वी पर हुआ होता तो धूल उतनी उंचाई तक नही उठ सकती थी ना ही धूलकण पैराबोलिक पथ पर उतनी तेजी से सतह पर गिरेगें।
2. अपोलो 15 अभियान मे डेविड स्काट ने एक हथौडे और एक चील के पंख को समान उंचाई से एक साथ गिराया था। दोनो एक ही गति से नीचे गिरे थे और सतह पर एक ही समय मे पहुंचे थे, यह दर्शाता है कि वे निर्वात मे थे।
- यदि चंद्रमा पर अवतरण को रेगिस्तान मे फ़िल्माया गया होता तो वीडियो मे ताप लहर(heat wave) स्पष्ट रूप से दिखाई देती।
यांत्रिकी समस्याये
1. ब्लास्ट क्रेटर: लुनर माड्युल द्वारा कोई गड्डा(Blast Crater) नही बना ना ही धूल उड़ाई!
निराकरण : लुनर माड्युल द्वारा किसी गड्डे के बनने की कोई संभावना ही नही थी। लुनर माड्युल के उतरते समय ही 10,000 पौंड के प्रणोद शक्ति वाले राकॆट इंजन को बहुत कम प्रणोद उत्पन्न करना पड़ा था। इसकी गति बहुत धीमी कम हो रही थी, उसे उतरते समय केवल अपने भार को ही सम्हालना था और चंद्रमा के कम गुरुत्व ने काम आसान कर दिया था। अवतरण के समय प्रणोद नोजल के पास केवल 10 किलोपास्कल या 1.5 PSI ही था।नोजल से निकलने के बाद उत्सर्जन फ़ैलता है और दबाव बहुत तेजी से कम हो जाता है। राकेट द्वारा उत्सर्जित गैस इंजन के नोजल से निकलने के बाद निर्वात मे पृथ्वी के वातावरण की तुलना मे अधिक तेजी से फ़ैलती है। राकेट की ज्वाला के वातावरण मे प्रभाव को पृथ्वी से राकेट के प्रक्षेपण के समय आसानी से देखा जा सकता है। जैसे ही राकेट घने वातावरण से उठकर पतले वातावरण मे पहुंचता है राकेट से उत्सर्जित ज्वाला अधिक फ़ैलती है। इस प्रभाव को कम करने के लिये राकेट के पतले वातावरण या निर्वात वाले स्टेज की नोजल को अधिक लंबाई वाले शंकु के रूप मे बनाया जाता है लेकिन इससे भी उनके फ़ैलने को पूरी तरह रोका नही जा सकता। इन प्रभाव के फ़लस्वरूप लुनर माड्युल से निकलने वाली गैस लैंडीग स्थल पर दूर तक तेजी से चौड़ाई मे फ़ैली। अवतरण इंजनो ने चंद्रमा की महीन धूल को उतरते समय उड़ाया इसे फ़िल्मो मे देखा भी जा सकता है लेकिन बहुत कम मात्रा मे। चंद्रमा पर उतरते समय लैंडर सीधे नीचे ना उतर कर धीमे धीमे क्षैतिज रूप से गति कर रहे थे और नीचे आ रहे थे, चित्रो मे लैंडर द्वारा उड़ाई गई धुल से इस पथ को भी देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त धूल की सतह के नीचे चंद्रमा की सतह बह्त कठोर है जिससे क्रेटर बनने की संभावना नही थी। अपोलो 11 के अवतरण स्थल पर बने ब्लास्ट क्रेटर की गहराई मापने पर पता चला था कि इंजन ने नोजल शंकु के नीचे केवल 4-6 इंच की ही धूल हटाई थी
![अपोलो 11 के लुनर लैंडर के नीचे का चित्र]()
अपोलो 11 के लूनर लैंडर के नीचे का चित्र
2. राकेट की अदृश्य ज्वाला प्रक्षेपण राकेट के द्वितिय चरण तथा लूनर माड्युल के राकेट की ज्वाला दृश्य नही थी।
निराकरण : लूनर माड्युल ने एअरोजीन 50 तथा डाईनाइट्रोजन टेट्रोक्साइड(आक्सीकारक) ईंधन का प्रयोग किया था। इन ईंधनो का चयन उनकी सरलता और भरोसेमंद होने के कारण किया गया था, इनके प्रज्ववलन के लिये चिंगारी की भी आवश्यकता नही है, दोनो एक दूसरे के संपर्क मे आते ही जल उठते है और पारदर्शी ज्वाला बनाते है। इसी ईंधन का प्रयोग टाईटन II राकेट मे हुआ था। इस ईंधन की ज्वाला के पारदर्शी होने की पुष्टि अन्य कई राकेट प्रक्षेपण चित्रो से की जा सकती है। निर्वात मे ईंधन की ज्वाला नोजल से निकलने के बाद तेजी से फ़ैलती है, जिससे उनका दिखाई देना और भी कठीन हो जाता है। अंतमे पृथ्वी के वातावरण मे राकेट ईंधन का कुछ भाग नोजल से निकलने के बाद वातावरण की आक्सीजन के साथ जलता है और ज्वाला दिखती है जोकि निर्वात मे संभव नही होता है।
![इस चित्र मे दर्शाये अनुसार राकेट से निकलने वाली ज्वाला अंतरिक्ष मे हमेशा दृश्य नही होती है। इन चित्र मे नीचे मध्य मे राकेट इंजन गहरे रंग की संरचना के रूप मे है।]()
इस चित्र मे दर्शाये अनुसार राकेट से निकलने वाली ज्वाला अंतरिक्ष मे हमेशा दृश्य नही होती है। इन चित्र मे नीचे मध्य मे राकेट इंजन गहरे रंग की संरचना के रूप मे है।
![टाईटन II राकेट का प्रक्षेपण जिसका इंधन hypergolic Aerozine-50/N2O4 है और इससे 1.9 MN प्रणोद उत्पन्न हो रहा है। ध्यान दिजिये की राकेट से निकलने वाली ज्वाला लगभग पारदर्शी है।]()
टाईटन II राकेट का प्रक्षेपण जिसका ईंधन hypergolic Aerozine-50/N2O4 है और इससे 1.9 MN प्रणोद उत्पन्न हो रहा है। ध्यान दीजिये की राकेट से निकलने वाली ज्वाला लगभग पारदर्शी है।
3 लुनर माडयुल के फ़ुटप्रिंट क्यों नही बने ?. लुनर माडयुल का भार 17 टन था लेकिन उसने चंद्रमा पर कोई निशान नही छोड़ा लेकिन उसके बाजू मे मानव पदचिह्न देखे जा सकते है।
निराकरण : पृथ्वी की सतह पर अपोलो 11 मे ईंधन भरा हुआ था, यात्रीयों के साथ इगल लुनर माड्युल का भार लगभग17 टन (15,300 किग्रा) था। लेकिन चंद्रमा की सतह पर अवतरण के बाद ईंधन जलाने के पश्चात उसका भार केवल 1224 किग्रा बचा था। चंद्रयात्रीयो का भार लुनर माड्युल की तुलना मे कम था लेकिन उनके बूट लुनर माड्युल के फ़ूटपैड (91 सेमी) की तुलना मे बहुत छोटे थे। अर्थात चंद्रयात्रीयों के पैर कम क्षेत्रफ़ल मे अधिक दबाव डाल रहे थे और जिससे उनके बूट के निशान स्पष्ट बने थे। लुनरमाड्युल के फ़ूटपैड के निशान भी बने और जो अन्य चित्रो मे दिख जाते है लेकिन वे उतने स्पष्ट नही है क्योंकि वे अधिक क्षेत्र मे दबाव डाल रहे थे।
![अपोलो 14 लुनर माड्युल]()
अपोलो 14 लुनर माड्युल
4. चंद्रयात्रीयों के सूट की वातावनुकूलन प्रणाली: निर्वात की परिस्थितियों मे कार्य नही कर सकती है।
निराकरण : चंद्रयात्रीयों के सूट की वातावनुकूलन प्रणाली केवल निर्वात मे ही कार्य कर सकती है। इस प्रणाली मे सूट के बैकपैक मे से पानी सूट की सतह वाली सबलिमिटर परत पर बने नन्हे छिद्रो से बाहर आता है और अंतरिक्ष मे बास्पीकृत हो जाता है। उष्मा की इस क्षति से शेष जल शीतल होकर बर्फ़ बन जाता था जोकि इस सबलिमिटर परत पर बर्फ़ की एक परत बना देता था। यह बर्फ़ सूट से उष्मा लेकर सबलिमिट होकर सीधे भाप मे बदल जाती थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य पानी की ट्युब अंतरिक्षयात्रीयों के जल द्वारा शीतलीकृत कपड़ो(LCG (Liquid Cooling Garment) ) से बहती थी जोकि यात्री की चयापचय क्रिया से उत्पन्न गर्मी हो बाह्य सबलिमटर प्लेट तक लेजाकर शीतल कर वापस आती थी। यात्रीयो के स्पेससूट मे 5.4 किग्रा जल से आठ घंटो का शीतलन प्राप्त होता था। यात्रीयों की यान बाह्य गतिविधियों के अधिक अंतराल के लिये यह एक बड़ी कठीनाई थी।
प्रसारण
1 संचार मे विलंब: पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य 400,000 किमी दूरी के कारण संचार मे दो सेकंड से अधिक का विलंब होना चाहीये।
निराकरण : पृथ्वी से चंद्रमा और चंद्रमा से पृथ्वी के मध्य संचार मे दो सेकंड से अधिक का विलंब सभी वास्तविक ध्वनि रिकार्डींग मे स्पष्ट है। लेकिन कुछ वृत्तचित्रो मे समय के बचाव तथा स्पष्टता के लिये इस विलंब को संपादन के दौरान हटा दिया गया है।
2. संचार मे विलंब केवल 0.5 सेकंड का था।
निराकरण : यदि हम वास्तविक ध्वनि रिकार्डींग को देखे तो स्पष्ट है संचार मे विलंब केवल 0.5 सेकंड के होने की बात पूर्णत : असत्य है। इसके अतिरिक्त यह विलंब हमेशा दोनो ओर एक जैसा नही है क्योंकि रिकार्डींग पृथ्वी के नियंत्रण कक्ष मे हो रही थी। नियंत्रण कक्ष द्वारा दिये गये उत्तर मे कोई विलंब नही है क्योंकि उनकी रिकार्डींग तत्काल हो रही है। चंद्रयात्रीयों द्वारा दिये गये उत्तरो मे विलंब स्पष्ट है।
3. आस्ट्रेलिया से प्रसारण योजना थी कि प्रथम चंद्रमा पर अवतरण का संचार आस्ट्रेलिया की पार्क्स वेधशाला(Parkes Observatory in Australia) से समस्त विश्व को रीले किये जायेंगे। लेकिन इस योजना को प्रथम चंद्रमा अवतरण से पांच घंटे पहले रद्द कर दिया गया।
निराकरण : चंद्रमा पर प्रथम कदम का समय चंद्रमा पर लुनर माड्युल के उतरने के बाद मे बदला गया था। यह विलंब इतना था कि पार्क्स वेधशाला इस संचार का रिले पूरे समय तक करने मे सक्षम नही थी।
4. पार्कस वेधशाला के विडियो संकेत : पार्कस वेधशाला के पास चंद्रमा से सबसे स्पष्ट वीडियो संकेत उपल्बध होना चाहिये थे लेकिन आस्ट्रेलियन मीडिया समेत सभी मीडिया स्रोतो ने अमरीका से लाईव फ़ीड प्रसारित किया।
निराकरण : वास्तविक योजना और आधिकारीक पालीसी के अनुसार आस्ट्रेलियन ब्राडकास्टींग कार्पोरेशन(ABC) ने संकेत पार्क्स वेधशाला तथा हनीस्क्ल क्रीक रेडीयो टेलिस्कोप (Honeysuckle Creek radio telescopes.)से सीधे लिये थे। इन संकेतो को NTSC टीवी संकेतो मे पैडींगटब सीडनी मे बदला गया था। इसका अर्थ यह भी है कि आस्ट्रेलियन दर्शको ने बाकी विश्व की तुलना मे चंद्रमा पर मानव अवतरण को कुछ सेकंड पहले देखा।
तकनीक
कांसपिरेसी थ्योरिस्ट बार्ट सिब्रेल के अनुसार यदि सोवियत संघ और अमरीका की अंतरिक्ष तकनीक क्षमताओं को देखें तो उस समय अमरीका के पास इस यात्रा के लिये आवश्यक तकनीक नही थी। अंतरिक्ष की इस दौड मे सोवियत संघ अमरीका से कोसों आगे था, इसके बावजूद सोवियत संघ चंद्रमा पर मानव उतारना तो दूर उसकी कक्षा मे भी कभी मानव नही भेज पाया। वे तर्क देते है कि जब सोवियत संघ बेहतर तकनीक होने के बावजूद चंद्रमा पर मानव नही भेज पाया तो अमरीका भी चंद्रमा पर मानव भेजने मे समर्थ नही होना चाहिये था।
उदाहरण के लिये वे कहते है कि अपोलो अभियान के दौरान तक सोवियत संघ के अंतरिक्ष यात्रीयो द्वारा अंतरिक्ष मे बिताया समय अमरीका की तुलना मे पांच गुना अधिक था। इसके अतिरिक्त सोवियत संघ अंतरिक्ष दौड मे बहुत से मील के पत्थरो मे प्रथम था जैसे पृथ्वी की कक्षा मे प्रथम मानव निर्मित उपग्रह(आक्टोबर 1957 स्पूतनिक), अंतरिक्ष मे प्रथम प्राणी( नवंवर 1957 स्पूतनिक 2 मे लाईका नामक कुतिया), अंतरिक्ष मे प्रथम मानव( अप्रैल 1961 वोस्तोक 1 मे युरी गागारीन), अंतरिक्ष मे प्रथम महिला (जुन 1963 वोस्तोक 6 मे वेलेंटीना टेरेश्कोवा), प्रथम अंतरिक्ष मे चहलकदमी/यान बाह्य गतिविधी (मार्च 1965 वोस्खोद 2 द्वारा अलेक्सेई लेनोव)।
लेकिन इस सभी सोवियत प्रथमो की बराबरी अमरीका ने एक वर्ष के अंदर ही कर ली थी, कुछ मामलो मे तो कुछ ही सप्ताहों के भीतर। 1965 मे तो अमरीका कुछ अंतरिक्ष गतिविधियों मे प्रथम हो गया था जैसे की पहला सफ़ल अंतरिक्ष यानो का जुड़ाव जो कि चंद्रमा तक अंतरिक्ष यात्रा मे अत्यावश्यक था। इसके अतिरिक्त नासा तथा अन्य एजेंसीयों के अनुसार सोवियत संघ द्वारा किये गये ये सभी प्रथम उतने अधिक प्रभावी नही थे जितने वे दिखाई देते है। इनमे से अधिकतर प्रथम तकनीकी रूप से बेहतर होने की बजाय स्टंट अधिक थे जैसे अंतरिक्ष मे प्रथम महिला। तथ्य यह है कि अपोलो अभियान की प्रथम मानव उड़ान अपोलो 7 तक सोवियत संघ ने केवल नौ मानव उड़ाने की थी जिसमे सात मे एक एक यात्री, एक मे दो यात्री और एक मे तीन यात्री थे, इस समय तक अमरीका ने 16 मानव उड़ाने भर ली थी। अंतरिक्ष मे बिताये समय के पैमाने पर सोवियत संघ ने अंतरिक्ष मे 460 घंटे बिताये थे जबकि अमरीका ने 1024 घंटे। यदि इसे मानव घंटो मे गिना जाये तो सोवियत संघ के 534 मानव अंतरिक्ष उड़ान घंटे थे, अमरीका के 1992 मानव अंतरिक्ष उड़ान घंटे। अपोलो 11 के आते तक अमरीका सोवियत संघ से बहुत आगे हो गया था।
इसके अतिरिक्त उस समय सोवियत संघ के पास मानव चंद्र अभियान के लायक शक्तिशाली राकेट नही था। 1969 से 1972 मे मध्य सोवियत संघ का राकेट N1 चार बार असफ़ल हुआ। 1970-1971 के मध्य सोवियत चंद्रयान LK की जांच उड़ान पृथ्वी की निम्न कक्षा मे तीन बार हुई थी।
चंद्रमा पर अवतरण के तृतिय पक्ष के प्रमाण
अवतरण स्थलो के चित्र
![लुनर रिकॉनिसैंस ओर्बीटर(Lunar Reconnaissance Orbiter) द्वारा अपोलो 17 की लैंडींग साईट के लिये चित्र]()
लुनर रिकॉनिसैंस ओर्बीटर(Lunar Reconnaissance Orbiter) द्वारा अपोलो 17 की लैंडिंग साईट के लिये चित्र
कांस्पिरेसी थ्योरिस्ट मानते है कि जमीनी वेधशाला तथा हब्बल टेलिस्कोप से अवतरण स्थलो के चित्र लेना संभव होना चाहिये। इसका अर्थ यह भी है कि इन लैंडीग जगहो के चित्र ना लेकर ये वेधशालाये और हब्बल टेलीस्कोप भी षडयंत्र मे सहभागी है। चंद्रमा पर अवतरण स्थलो के चित्र हब्बल टेलिस्कोप ने लिये है लेकिन हब्बल टेलिस्कोप के चित्रो का रिजाल्युशन इतना कम है कि उसमे चंद्रमा 55-69 मीटर से कम चौड़ी वस्तुओ को पहचाना नही जा सकता है।
अप्रैल 2001 मे लिओनार्ड डेवीड ने space.com पर एक लेख मे एक क्लेमेंटाईन अभियान(Clementine mission) द्वारा लिया गया एक चित्र दिखाया था जो कि नासा के अनुसार अपोलो 15 का लैंडर था। इस चित्र को ब्राउन विश्वविद्यालय(Brown University) के भूगर्भ शास्त्र विभाग(Department of Geological Sciences) की मिशा क्रेस्लावस्की(Misha Kreslavsky) तथा खार्कीव खगोल वेधशाला युक्रेन(Kharkiv Astronomical Observatory in Ukraine.) की युरी श्कुरावतोव(Yuri Shkuratov) ने पहचाना था। युरोपियन अंतरिक्ष संस्थान (European Space Agency’s )के स्मार्ट 1(SMART-1 ) मानवरहित शोधयान ने लैंडिंग साईट के चित्र लिये थे।
2002 मे हवाई विश्वविद्यालय(University of Hawaii ) के अलेक्स आर ब्लैक्वेल चंद्रमा की कक्षा मे रहते हुये अपोलो अंतरिक्ष यात्रीयों के द्वारा लिये गये चित्रो मे अपोलो लैंडीग साईट को पहचाना था।
14 सितंबर 2007 ko जापान अंतरिक्ष संस्थान(The Japan Aerospace Exploration Agency) (JAXA) ) ने सेलेन चंद्रयान(SELENE Moon orbiter) प्रक्षेपित किया था। यह चंद्रयान चंद्रमा की सतह से 100 किमी उंचाई पर परिक्रमा कर रहा था। मई 2008 मे इस संस्थान से लिये गये चित्रो मे अपोलो 15 के इंजन एक्सहास्ट को देखा।
17 जुलाई 2009 मे नासा ने लुनर रिकॉनिसैंस ओर्बीटर(Lunar Reconnaissance Orbiter) द्वारा अपोलो 11,14,15,16,17 की लैंडींग साईटो के लिये चित्र प्रकाशित किये। इन चित्रो मे चंद्र्मा की सतह पर सभी अभियानो के लुनर लैंडर के अवतरण इंजनो को देखा जा सकता है। इन चित्रो मे अपोलो 14 के यात्रीयो द्वारा किये गये एक प्रयोग ALSEP के दौरान बनाये गये पदचिह्नो के ट्रेक को भी देखा जा सकता है। नासा ने 3सितंबर 2009 को अपोलो 12 के अवतरण स्थल के चित्रो को प्रकाशित किया, इन चित्रो मे सर्वेयर 3 यान, ALSEP प्रयोग के उपकरण और चंद्रयात्रीयों के पद चिह्न स्पष्ट रूप से दिखाई देते है। इन चित्रो से वैज्ञानिक समुदाय तो उत्साहित हुआ लेकिन कांसपिरेसी थ्योरीस्ट पर कोई प्रभाव नही पड़ा।
1 सितंबर 2009 को भारत के चंद्र अभियान चंद्रयान 1 (Chandrayaan-1)ने अपोलो 15 के अवतरण स्थल और चंद्रवाहन(Lunar Rover) के ट्रेक के चित्र लिये। भारतीय अंतरिक्ष संस्थान(Indian Space Research Organisation ) ने यह अभियान सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 8 सितंबर 2008 को प्रक्षेपित किया था। इन चित्रो को चंद्रयान के हायपरस्पेक्ट्रल कैमरे(hyperspectral camera) ने लिया था।
2010 मे प्रक्षेपित चीन के दूसरे चंद्रयान अभियान चांग 2 (Chang’e 2) की क्षमता 1.3 मिटर रिजाल्युशन की है। उसने भी अपोलो लैंडीग स्थलो के चित्र लिये और लैंडरो द्वारा छोड़े चिह्नो को पहचाना।
चंद्रमा से लाई गई चट्टाने
![चंद्रमा से लाई जिनेसीस चट्टान]()
चंद्रमा से लाई जिनेसीस चट्टान
समूचे अपोलो कार्यक्रम के दौरान छह मानव अभियान से चंद्रमा से 380 किलोग्राम चट्टानी टूकड़े लाये गये। समस्त विश्व के वैज्ञानिको द्वारा इन चट्टानो का अध्ययन किया गया, समस्त वैज्ञानिक मानते है कि ये चट्टाने चंद्रमा से आई है, अब तक किसी भी जनरल मे एक भी ऐसा शोधपत्र प्रकाशित नही हुआ है जो इस दावे पर प्रश्न उठाता हो। अपोलो कार्यक्रम द्वारा लाई गई चट्टाने उल्काओं तथा पृथ्वी की चट्टानो से संरचना मे भिन्न है। इन चट्टानो मे पृथ्वी की चट्टानो के जैसे जल का असर नही है। इन चट्टानो मे निर्वात मे होने वाली टक्करो का प्रभाव स्पष्ट है, साथ मे यह चट्टाने पृथ्वी की चट्टानो से 20 करोड़ वर्ष पुरानी है। ये चट्टाने सोवियत संघ द्वारा लाई गई चट्टानो के जैसे ही है।
कांसपिरेसी थ्योरीस्ट कहते है कि अपोलो 11 अभियान से दो वर्ष पहले 1967 मे मार्शल स्पेस फ़्लाईट सेंटर के निदेशक वेर्नेर वान बरुन (that Marshall Space Flight Center Director Wernher von Braun’s )अंटार्कटिका गये थे, उन्होने चंद्रमा से पृथ्वी पर आई उल्काये जमा की थी जिन्हे अपोलो अभियान द्वारा चंद्रमा से लाई गई चट्टानो के रूप मे दिखाया गया। वान बरुन नाजी अफ़सर थे, इसलिये कांसपिरेसी थ्योरिस्ट कहते है कि उन्हे अपने भूतकाल के कर्मो की सजा से बचने के लिये इस षडयंत्र का भाग बनने के लिये मजबूर किया गया। नासा के अनुसार वान बरुन का अभियान भविष्य के अंतरिक्ष अभियानो के लिये वातावरण और तार्किक कारको की खोज करने के लिये था। नासा अब भी अपनी टीमो को अन्य ग्रहों की परिस्थिति से मिलती जुलती परिस्थितियों की तैयारीयों के लिये अंटार्कटीका भेजता है।
अब वैज्ञानिक समुदाय इस बात पर एकमत है कि मंगल और चंद्रमा पर क्षुद्रग्रहों के टकराव से अंतरिक्ष मे उछलने वाला मलबा उल्काओं के रूप मे पृथ्वी पर गिरता है। लेकिन इस तरह की सबसे पहली चंद्र-उल्का 1979 मे पाई गई थी तथा उसके वास्तविक स्रोत की पहचान 1982 तक नही हुई थी। इसके अतिरिक्त चंद्र उल्काये इतनी दुर्लभ है कि किसी भी हालत मे समस्त पृथ्वी से 1969-72 के मध्य तक 380 किलो चंद्र उल्काये जमा नही की जा सकती है। निजी उल्का जमाकर्ताओ, सरकारी एजेंसीयों की 20 वर्ष की मेहनत के बाद भी अब तक समस्त विश्व मे केवल 30 किलो चंद्र उल्काये पाई गई है।
![अपोलो अंतरिक्ष अभियानो ने 380 किलो चंद्र चट्टाने जमा की, जबकि सोवियत रोबोटिक अभियान लुना 16, लुना 20 तथा लुना 24 ने कुल मिलाकर मात्र 326 ग्राम चंद्र उल्का जमा कर ला पाये जोकि अमरीकी अभियान के हजारवे भाग से भी कम है।]()
अपोलो अंतरिक्ष अभियानो ने 380 किलो चंद्र चट्टाने जमा की, जबकि सोवियत रोबोटिक अभियान लुना 16, लुना 20 तथा लुना 24 ने कुल मिलाकर मात्र 326 ग्राम चंद्र उल्का जमा कर ला पाये जोकि अमरीकी अभियान के हजारवे भाग से भी कम है।
अपोलो अंतरिक्ष अभियानो ने 380 किलो चंद्र चट्टाने जमा की, जबकि सोवियत रोबोटिक अभियान लुना 16, लुना 20 तथा लुना 24 ने कुल मिलाकर मात्र 326 ग्राम चंद्र उल्का जमा कर ला पाये जोकि अमरीकी अभियान के हजारवे भाग से भी कम है। वर्तमान की योजनाओं के अनुसार मंगल से चट्टान जमा कर पृथ्वी पर तक लाने का अभियान का लक्ष्य केवल 500 ग्राम का है, दूसरी ओर प्रस्तावित साउथपोल ऐटकेन बेसीन रोबोटीक(South Pole-Aitken basin) अभियान चंद्रमा से केवल 1 किलो चट्टान जमा कर पायेगा। यदि नासा ने रोबोटिक अभियानो के प्रयोग से इतनी मात्रा मे चंद्र चट्टाने जमा कर लाई होती थो उसे 300-2000 अभियान भेजने पड़े होते।
चंद्रमा की चट्टानो की संरचना पर कांसपिरेसी थ्योरीस्ट कायसिंग पुछते है कि “चंद्रमा की चट्टानो सोना, चांदी, हीरे या अन्य बहुमुल्य धातुओं की चर्चा क्यों नही होती है ? क्या यह महत्वपूर्ण नही है ? इन बातो की चर्चा किसी प्रेस कांफ़्रेस मे किसी चंद्रयात्री ने क्यों नही की ?” भूगर्भशास्त्री मानते है कि पृथ्वी के गर्भ मे स्वर्ण और चांदी के भंडार भूगर्भीय उष्मा के द्वारा पिघल कर कुछ विशेष स्थानो पर जमा हुये है। इसतरह के भंडारो का निर्माण चंद्रमा पर मिलना कठिन है और मिल भी जाये तो उन्हे पृथ्वी तक लाना अत्यधिक महंगा पड़ेगा।
स्वतंत्र पक्षो द्वारा इन अभियानो का निरिक्षण
नासा के अतिरिक्त बहुत से समूहो और व्यक्तियों ने अपोलो अभियान पर कड़ी नजर रखी थी। बाद के अभियानो मे नासा ने समय समय पर इन यानो के दिखाई देने के समय और स्थान की पूर्व सूचना दी थी। कई समूहो ने इन यानो के उड़ान पथ पर राडारो से नजर रखी थी, दूरबीनो से चित्र लिये थे। इसके अतिरिक्त पृथ्वी के नियंत्रण कक्ष से यानो मे मध्य के रेडीयो संवादो को स्वतंत्र रूप से रिकार्ड किया था।
रेट्रोरिफ़्लेक्टर
![अपोलो 11 का रेट्रोरिफ़्लेक्टर]()
अपोलो 11 का रेट्रोरिफ़्लेक्टर
अपोलो अभियान चंद्रमा पर कुछ विशेष लेजर परावर्तक(रेट्रोरिफ़्लेक्टर) छोड़ कर आये है। इन रिफ़्लेक्टरो पर पृथ्वी से लेजर किरणे भेज कर उन्हे वापिस पृथ्वी पर ग्रहण किया जा सकता है। लिक वेधशाला(Lick Observatory ) ने यह प्रयोग अपोलो 11 के समय पर किया था जब नील आर्मस्ट्रांग और बज आल्ड्रीन चंद्रमा की सतह पर ही थे लेकिन उन्हे सफ़लता 1 अगस्त 1969 को ही मिल पाई थी। अपोलो 14 ने 5 फ़रवरी 1971 को चंद्रमा पर रिफ़्लेक्टर छोडे थे जिन्हे मैकडोनाल्ड वेधशाला(McDonald Observatory) ने उसी दिन जांचा था। अपोलो 15 के रिफ़्लेक्टर 31 जुलाई 1971 को स्थापित हुये थे जिसे मैकडोनाल्ड वेधशाला ने अगले कुछ दिनो मे खोज लिया था। इसके अलावा कुछ छोटे रिफ़्लेक्टर सोवियत रोबोटिक अभियान लुनोखोद 1(Lunokhod 1) तथा 2 (Lunokhod 2) ने भी स्थापित किये है।
अपोलो अभियान के बाद मानव चन्द्रमा पर क्यों नही गया?
रोबोटिक अभियान सस्ते, सुरक्षित और बेहतर होते है। मानव अभियानो मे मानव को भेजने के अतिरिक्त उनके खाने, पीने, जीवित रहने का इंतजाम तो करना ही होता है। इसके साथ ही उन्हे वापस लाने का भी इंतजाम करना होता है। हर कदम पर यात्रीयों की जान का खतरा भी बना होता है। रोबोटिक अभियान एक तरफ़ा होते है उन्हे वापस लाने का इंतजाम नही करना होता है।
दूसरा यह है रोबोटिक अभियान को वापस लाने की बाध्यता ना होने से वे लंबे समय तक कार्य करते रह सकते है।
अब आते है अन्य तथ्यो पर
![सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अपोलो अभियान वैज्ञानिक अभियान कभी था ही नही!]()
सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अपोलो अभियान वैज्ञानिक अभियान कभी था ही नही!
सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अपोलो अभियान वैज्ञानिक अभियान कभी था ही नही!
कुल एक दर्जन चन्द्रयात्रियों में से केवल एक वैज्ञानिक चन्द्रमा पर गया था, वह भी अंतिम चन्द्र अभियान में, बाकी सभी सैन्य अधिकारी थे।
वैज्ञानिक इतनी निरीह प्रजाति है कि उनके हाथों में यह अधिकार कभी नही रहा जिससे वे चयन कर पाए कि शोध की दिशा क्या हो! इन शोध के लिए पैसों का निर्णय राजनेता लेते है, वे ही दिशा देते है। राजनेताओं की प्राथमिकता विज्ञान नही अगले चुनाव होते है।
यह अभियान एक सैन्य राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई थी, नाक की लड़ाई थी। एक राजनेता द्वारा दशक के अंत तक चन्द्रमा पर मानव भेजने की सनक का परिणाम था। अपोलो यान सुरक्षित नही थे, तीन यात्रियों की मौत प्रयोग के दौरान एक दुर्घटना में जल कर हुई थी, तीन अंतरिक्ष यात्री अपोलो 13 में मरते मरते बचे थे।
सोवियत संघ अंतरिक्ष मे उपग्रह भेजने में, प्राणी भेजने में, मानव भेजने में, तकनीक में अमरीका से आगे और बेहतर था। तकनीक में अब भी बेहतर है। (नासा के कई तरह के यान, शटल रिटायर हो गए, सोयुज अब भी सुरक्षित माना जाता है।)
ऐसे में अमरीकी मानसिकता असुरक्षित महसूस कर रही थी, राजनेता अलोकप्रिय हो रहे थे। केनेडी ने इसमें राजनीतिक सम्भावनाएं देखी इसको चुनौती की तरह पेश कर चाँद यात्रा की घोषणा कर दी जिसके फलस्वरूप अपोलो अभियान सामने आया। आखिर मानव ने चन्द्रमा पर अपने कदम रख दिये। आगे ? आगे कुछ नही क्योंकि मानव अभियान से अधिक हासिल कर पाने की हालत में मानव ना तब था ना अब है। जब नेताओ ने देखा कि जनता का ध्यान अपोलो, चन्द्रमा से हट गया है, बाकी के अभियानों के लिए नासा की फंडिंग बन्द कर दी गयी फलस्वरूप अपोलो 18,19,20 कचरे के डिब्बे में डाल दिये गए। अपोलो 18 तो पूरी तरह से तैयार था।
अंतरखगोलीय मानव अभियान लम्बे हो भी नही हो सकते, खाने पीने रहने, सुरक्षित जाने आने की तैयारी चुनौती मुश्किल होती है। इसलिए अब अभियान केवल रोबोटिक होते है। मार्स रोवरों जैसी वैज्ञानिक सफ़लता मानव अभियान अब भी हासिल नही कर सकते।
एक बार पिछड़ने के बाद सोवियत संघ ने चन्द्रमा पर मानव भेजने का प्रयास कभी नही किया, बाद में पता चला कि मानव अभियान उनकी प्राथमिकता में था ही नही। वे सेल्यूट और उसके बाद मीर में ही खुश थे।
इस विषय पर खगोल वैज्ञानिक निल डिग्रेस टायसन को सुनिए
सारांश
यह एक तथ्य है कि अपोलो 11 अभियान द्वारा मानव ने चंद्रमा पर कदम रखे थे। लेकिन कांसपिरेसी थ्योरिस्ट इसपर भरोसा नही करंगे, चाहे उनके सामने कितने भी प्रमाण रख दिये जाये। आम लोगो को यह समझने की आवश्यकता है कि कांसपिरेसी थ्योरी एक बड़ा व्यवसाय बन चुका है, इन थ्योरी पर आधारित पुस्तके लिखी जाती है, उनकी बिक्री होती है। टीवी पर डाक्युमेंट्री दिखाई जाती है और उसके विज्ञापनो से कमाई होती है। इंटरनेट के जमाने मे ऐसी कांसपिरेसी थ्योरी की बदौलत वेबसाईट चलती है, विज्ञापन से आय होती है। युट्युब जैसे विडियो चैनल पर अधिक से अधिक लोगो को आकर्षित करने मे इस तरह की कांसपिरेसी थ्योरी बड़ा आकर्षण होती है।
अंत मे हम यही कहेंगे कि इंटरनेट, टीवी पर आंख मूंदकर भरोसा मत कीजिये, तर्को और तथ्यो को प्रमाणो की कसौटी पर जांच कर ही भरोसा करें।
इस विषय पर कुछ अन्य वेबसाईट/डाक्युमेंटरी
- खगोलशास्त्री फ़िल प्लेट का बैड आस्ट्रोनामी : http://www.badastronomy.com/bad/tv/foxapollo.html
- इस कांसपिरेसी थ्योरी का खंडन करने समर्पित साईट :http://www.clavius.org/
- टीवी धारावाहिक मिथबस्टर का इस विषय पर पूरा एपिसोड :https://www.dailymotion.com/video/x2m7k1z
- इस थ्योरी की धज्जीयाँ उड़ाता रैशनलविकी का लेख https://rationalwiki.org/wiki/Moon_landing_hoax
- विकिपिडीया पर लेख : https://en.wikipedia.org/wiki/Moon_landing_conspiracy_theories
- http://earthsky.org/space/apollo-and-the-moon-landing-hoax
- https://www.space.com/12814-top-10-apollo-moon-landing-hoax-theories.html
- https://www.washingtonpost.com/news/speaking-of-science/wp/2018/07/20/why-do-people-believe-the-moon-landing-hoax-or-other-conspiracy-theories/?noredirect=on&utm_term=.ff2ba1973115



































!["एक मानव का एक छोटा कदम, मानवता के लिये एक बड़ी छलांग है। (दैट्स वन स्माल स्टेप ऑफ़ [अ] मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड)"](http://vigyan.files.wordpress.com/2015/07/comments.png?w=300&h=16)